
‘कंट्रोल+कमांड’ वाली भारत सरकार का ब्याज दरों पर अजीब रवैया क्यों
आजादी के बाद चार दशकों से ज्यादा हमारी सरकारों ने ब्याज दरों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.
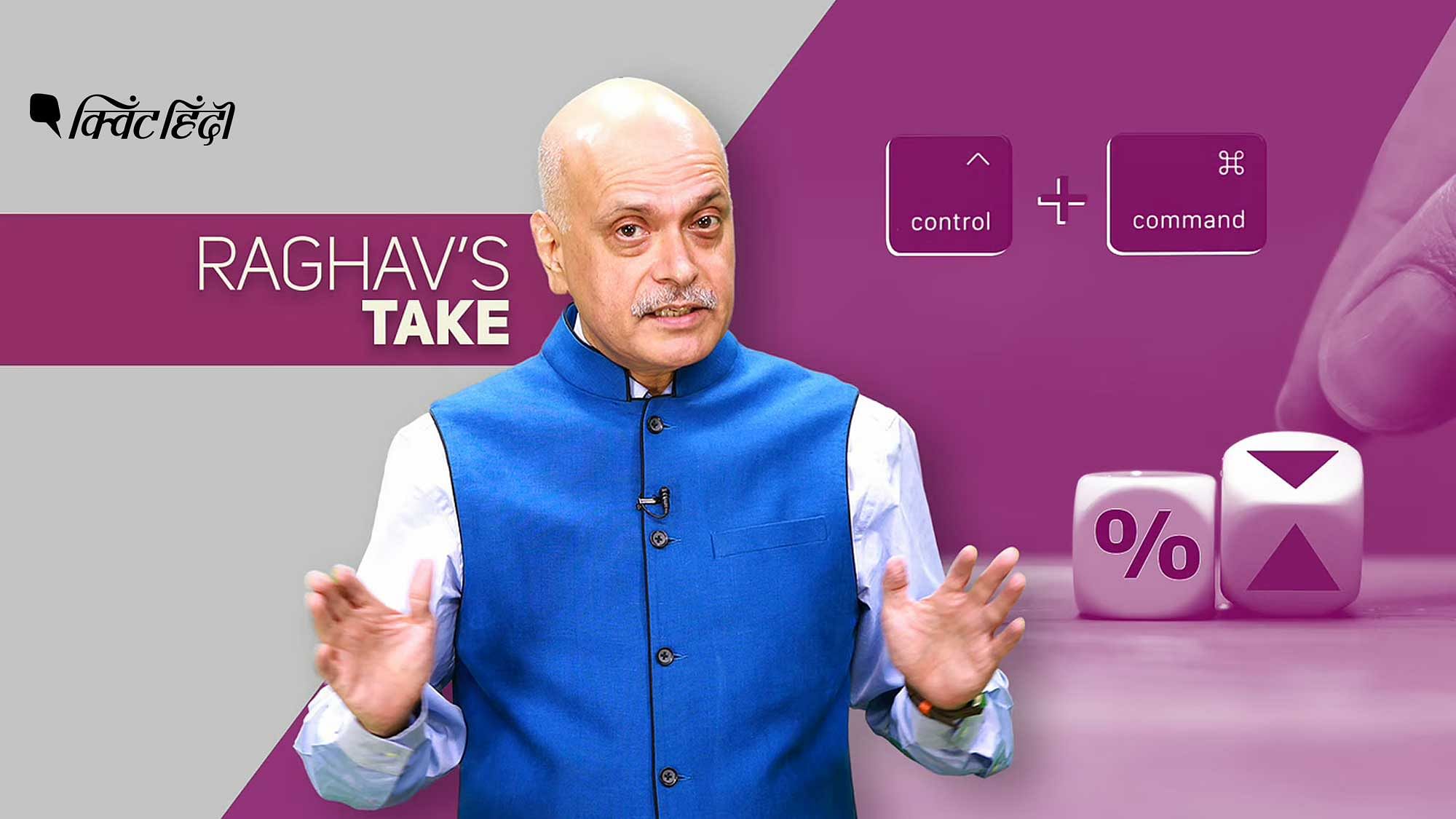
advertisement
किसी भी भारतीय नेता से ये सवाल पूछिए: “अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कीमत किसकी है?”
तुरंत जवाब मिलेगा: “प्याज की कीमत, क्योंकि ये सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है.”
अब अगर सवाल ये पूछें कि: लेकिन आर्थिक सिद्धांत के मुताबिक तो ये ब्याज दरें हैं यानी पैसे की कीमत ज्यादा महत्वपूर्ण है. ”
इसके बाद आपका अभिवादन आश्चर्य से भरे एक चेहरे से होगा जो करीब-करीब ये कहता है कि: “मूर्ख मत बनो! ब्याज दरें वो हैं जो बैंक मेरे फिक्स्ड डिपोजिट पर देती हैं. पैसे की ‘कीमत’ होने का क्या बकवास है? पैसा वो कीमत है, जो मैं प्याज खरीदने के लिए देता हूं. तो पैसे की अपनी कीमत कैसे हो सकती है?”
मेरे प्यारे पाठकों, यही वो समस्या है जो देश को सता रही है. आजादी के बाद चार दशकों से ज्यादा हमारी सरकारों ने ब्याज दरों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. दरअसल 90 के दशक में जब तक इसपर से नियंत्रण हटाया नहीं गया था, तब तक सबकुछ सरकार के आदेश से तय किया जाता था.
आपके सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपोजिट, प्रोविंडेंड फंड, कार फायनांस, बिजनेस लोन सब कुछ की ब्याज दर सरकार तय करती थी. शायद इसी कारण से आज भी भारत सरकार के सभी स्तंभ- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और यहां तक कि मीडिया भी इसे मार्केट वैरिएबल की तरह नहीं लेता है, जैसा किसी भी नियंत्रित बाजार में किसी भी कीमत को प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय किया जाता है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूलने की ये राष्ट्रीय बीमारी पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है.
“ब्याज पर ब्याज” का ये जुनून क्यों?
देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखे मामले की सुनवाई चल रही है. ‘समस्या’ उस समय शुरू हुई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छह महीने के लिए कर्ज लिए गए पैसों पर दिए जाने वाले ब्याज पर रोक लगा दी. कोविड 19 के कारण जिनके व्यवसाय और कमाई का जरिया खत्म हो गए थे वैसे कर्जदारों को बचाने के नेक उद्देश्य से लिया गया ये एक जरूरी फैसला था.
जैसा कि किसी भी आपात स्थिति में होता है ये माना गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो ब्याज को उचित तरीके से ग्राहकों से वसूल लिया जाएगा. इसलिए ये सोचना स्वभाविक था कि देर से दिया जाने वाला ब्याज बकाया कर्ज में जुड़ जाएगा-एक उदाहरण के तौर पर, अगर मैंने 1,00,000 रुपये के लोन पर 10,000 का ब्याज नहीं चुकाया तो मेरा ‘नया लोन’ खुद बखुद 1,10,000 रुपये का हो जाएगा. और जब मोराटोरियम खत्म होगा तो मैं बढ़े हुए लोन यानी 1,10,000 रुपये चुकाने के लिए नया रीपेमेंट शेड्यूल बनाऊंगा. आम तौर पर ऐसा ही होता है. काम पर ‘ब्याज जुड़ने ’(इंट्रेस्ट कंपाउंडिंग) का सालों से यही सिद्धांत चला आ रहा है लेकिन उसके लिए नकारात्मक अर्थ में जो व्यक्ति ब्याज दे रहा और उससे कमाई नहीं कर रहा है.
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था. कुछ याचिकाकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने एक तरह से बैंकों पर सूदखोर होने और शोषण करने के आरोप लगाए. उनका सवाल था कि “बैंक ब्याज पर ब्याज कैसे ले सकते हैं”. कई समझदार लोगों ने उन्हें इसका कारण बताने की कोशिश की-
- ये “ब्याज पर ब्याज” नहीं है- ये न चुकाए गए ब्याज पर लेवी है जो कि किसी भी दूसरे बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज की तरह है, और
- क्या होगा अगर आप कर्ज देने वाले/ जमाकर्ता हैं, और कर्ज लेने वाले नहीं हैं? अगर बैंक आपको ब्याज की एक किश्त नहीं दे सके तो क्या आप अतिरिक्त हर्जाना नहीं मांगेंगे? क्या ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत नहीं है? इसलिए अगर आपको अपनी कमाई पर इसे मांगने का हक है तो कर्ज पर इसे चुकाने का दायित्व क्यों नहीं है, और
- एक बार उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने इस सुविधा का फायदा नहीं लिया और कोविड 19 मोराटोरियम में भी समय पर लोन की किश्त चुकाता रहा. उसे उसकी ईमानदारी और अनुशासन के लिए क्यों भुगतना पड़े?
जवाब एकदम साफ थे, पूरी तरह से स्पष्ट. बिना किसी विवाद के वर्षों से चले आ रहे ‘कंपाउंडिंग’ के तर्क से माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दिन इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए था. लेकिन हम जैसे कई लोग हैरान थे.
इससे भी बुरा ये है कि ये करीब-करीब आम, सीधे-साधे और बेआवाज डिपोजिटर्स के भाग्य को नजरअंदाज कर रही है. ये बात मुझे हैरान करती है कि शक्तिशाली भारत सरकार-कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया-पूरी तरह से खोखले और ऐसे तर्क जिनकी रक्षा नहीं की जा सके, के पीछे अनगिनत घंटे समय दे रहे हैं जबकि लाखों आवश्यक मुद्दे भरे पड़े हैं. कुछ चीजें (अफसोस) सिर्फ भारत में होती हैं.
‘नए भारत’ में आपको आय पर ब्याज देना पड़ सकता है, कमाई नहीं होगी!
अब, अगर आपको लगता है कि “ब्याज पर ब्याज” की नाकामी आर्थिक निरक्षरता का एकमात्र उदाहरण है तो एक कठिनाई भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए. यहां तीन और बातों की चर्चा करते हैं जो इतने ही तर्कहीन हैं:
- जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को राजस्व देने की गारंटी दी थी. अब मोदी सरकार ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस वादे को पूरा करने के लिए उनके पास 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी है. लेकिन कोविड 19 की अव्यवस्था को ‘ऐक्ट ऑफ गॉड’ (जो कि साधारण कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी बचाव है) बताकर सरकार ने हार मानते हुए अड़ियल रवैये के साथ कहा कि “हम आपको पैसे नहीं दे सकते”. इसके बदले में आप सीधे बाजार से पैसे उधार लें और मूलधन को बाद में किसी सेस से वापस लें. इतना ही नहीं, इस लोन पर ब्याज भी राज्यों को ही देना होगा. ये अजीब है, शायदा दुनिया में इकलौता ऐसा उदाहरण जहां एक संस्था को अपनी वैध आय पर ब्याज देने कहा जा रहा है न कि कमाई करने के लिए!! ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि सबसे ज्यादा अहम मैक्रो-इकोनॉमिक वैरिएबल ब्याज दरों के तर्क को लेकर हमारी सरकार की प्रणाली कितनी अनजान है.
- गरीबों और कर्मचारी वर्ग के हितों की बात करने वालों को ये ठीक नहीं लगेगा लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 फीसदी का गारंटीड रिटर्न देना भी इतना ही अजीब है बावजूद इसके कि इस फंड को एक लाख करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ हो. हालांकि जमाकर्ताओं के साथ मेरी सहानुभूति है जिनके पैसों का इस्तेमाल इतने गलत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन 6 फीसदी (यानी मौजूदा 10 वर्षीय ट्रेजरी दर) के “जोखिम रहित” बेंचमार्क के ऊपर 250 बेसिस प्वाइंट की मांग में कोई आर्थिक तर्क नहीं है.
- अंत में अविश्वनीय रूप से विचित्र (हां, एक बार फिर) सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस-योग्य एजीआर की गणना करते समय वित्तीय साधनों पर ब्याज को शामिल करने का आदेश दिया- जो कि साफ तौर पर “नॉन ऑपरेटिंग इनकम” है. देखिए ये कितना विकृत है-एक कंपनी जो ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल करती है और इसलिए बैलेंस शीट में ज्यादा कैश सरप्लस रखती है, उसे दूसरी कंपनी जिसका इक्विटी बेस कम है और कर्ज में है, की तुलना में ज्यादा लाइसेंस फीस देना पड़ेगा. विचित्र!!! कुछ चीजें (टुट टुट) सिर्फ भारत में ही होती हैं.
अब, मैं यहां अपनी बात खत्म करता हूं. भारत सरकार की एक कमजोरी है. सरकार ये समझ नहीं सकी है कि ब्याज दर एक राजनीतिक हथियार नहीं है बल्कि प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में सबसे जरूरी कीमत है. यही कारण है कि ये एक वास्तविक बाजार अर्थव्यवस्था बनने के चारों ओर लड़खड़ाती, गिरती पड़ती रहती है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)
- साइट पर सभी पेड कंटेंट का एक्सेस
- क्विंट पर बिना ऐड के सबकुछ पढ़ें
- स्पेशल प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्रीव्यू